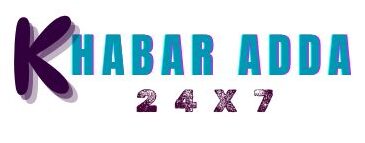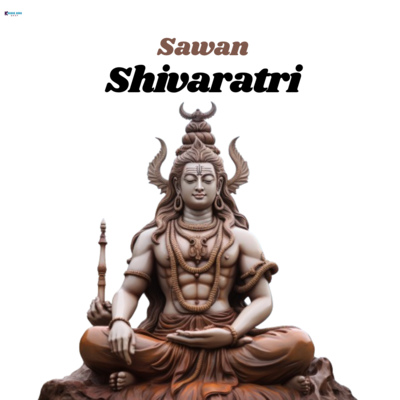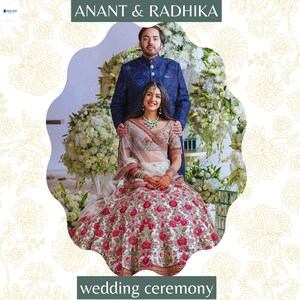Supreme Court of India संविधान का अंतिम व्याख्याता है और अपनी रचनात्मक और नवीन व्याख्या के माध्यम से हमारे संवैधानिक अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का रक्षक रहा है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के सिद्धांत या धारा 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति दी जाएगी।
In Short
Toggleभारत के Supreme Court का इतिहास
भारत के Supreme Court की उत्पत्ति औपनिवेशिक युग में हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में Supreme Court की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद, भारत की संविधान सभा ने एक न्यायिक निकाय की कल्पना की जो सेवा प्रदान करेगी। संविधान के संरक्षक के रूप में और न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कायम रखें। इस प्रकार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नव स्वतंत्र राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अस्तित्व में आया।
Supreme Court of India की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, भारत के संविधान के तहत, शीर्ष न्यायालय संविधान की व्याख्या करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का सर्वोपरि अधिकार रखता है। दशकों से, इसने देश के कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
क्या Supreme Court of India विश्वसनीय है?
एक भरोसेमंद न्यायालय की विशेषता उपलब्धता और स्पष्टता है की जो यह आश्वासन देता है कि न्याय न केवल दिया जाता है, बल्कि निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित भी माना जाता है। एक न्यायालय के सिद्धांतों में से एक इसकी राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना अधीक्षक और विधान सभा के अतिरेक के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक निष्पक्ष न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करता है।
कॉलेजियम प्रणाली या अन्य तंत्रों के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का उद्देश्य Supreme Court को राजनीतिक बाधा से अलग करना और उसकी स्वायत्तता को बचाना है। फिर भी, नियुक्ति प्रक्रिया में अधीक्षक और परिषद के प्रभाव के संबंध में शिकायतें उठाई गई हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर दबाव डाला गया है।
भारत में Supreme Court के निर्णय को कौन बदल सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दो तरह से चुनौती दी जा सकती है:
विधायी कार्रवाई: भारत की संसद को भारत के क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति है। ऐसे उदाहरण हैं जहां संसद ने नया कानून बनाकर या मौजूदा कानून में संशोधन करके अदालत के फैसले को पलट दिया है।
न्यायिक कार्रवाई: सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने फैसले की समीक्षा करके या उसे बड़ी पीठ के पास भेजकर उसे पलटने की शक्ति है।
अनुच्छेद 137:
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करना: संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी।
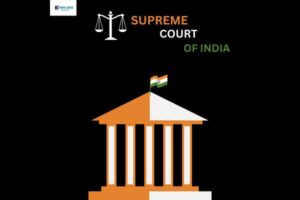
Supreme Court के महत्वपूर्ण 5 निर्णय
शंकर प्रसाद मामला बनाम भारत संघ (1951) :
यह मामला मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित था। Supreme Court ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की संसद की शक्ति में संविधान के भाग III में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।
बेरूबारी यूनियन केस बनाम अज्ञात (1980):
यह मामला बाबरी के क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने की संसद की शक्ति के संबंध में था। Supreme Court ने अनुच्छेद 3 की विस्तार से जांच की और माना कि नेहरू दोपहर समझौते को निष्पादित करने के लिए पक्ष इस अनुच्छेद के तहत कानून नहीं बना सकता है। इसलिए समझौते को लागू करने के लिए 9वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया।
गोलखनाथ मामला बनाम पंजाब राज्य (1967):
इस मामले में सवाल यह था कि क्या संशोधन एक कानून है और क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। Supreme Court ने तर्क दिया कि मौलिक अधिकार संसदीय प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं जैसा कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है और मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए एक नई संविधान सभा की आवश्यकता होगी। यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया देता है लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।
केशवनदा भारती बनाम केरल राज्य (1973):
संविधान के हड़पने के खिलाफ सुरक्षा के रूप में बुनियादी संरचना सिद्धांत का प्रचार। यह इस कारण से अद्वितीय था कि इसने लोकतांत्रिक शक्ति के संतुलन में बदलाव लाया। पहले के निर्णयों में यह रुख अपनाया गया था कि संसद एक उचित विधायी प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है।
न्यायालय द्वारा तैयार किया गया बुनियादी संरचना सिद्धांत न्यायिक रचनात्मकता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर के अन्य संवैधानिक न्यायालयों के लिए एक मानक स्थापित करता है।सिद्धांत ने फैसला सुनाया कि एक संवैधानिक संशोधन भी अमान्य हो सकता है यदि यह आवश्यक विशेषताओं को ख़राब करता है।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ(1978):
इसने भारत के संविधान के तहत “जीवन के अधिकार” के अर्थ का विस्तार किया। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहता है: किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।दूसरे शब्दों में, अदालतों को किसी भी कानून पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं थी, चाहे वह कितना भी मनमाना या दमनकारी क्यों न हो, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता हो, यदि कानून उपयुक्त रूप से पारित और अधिनियमित किया गया हो।